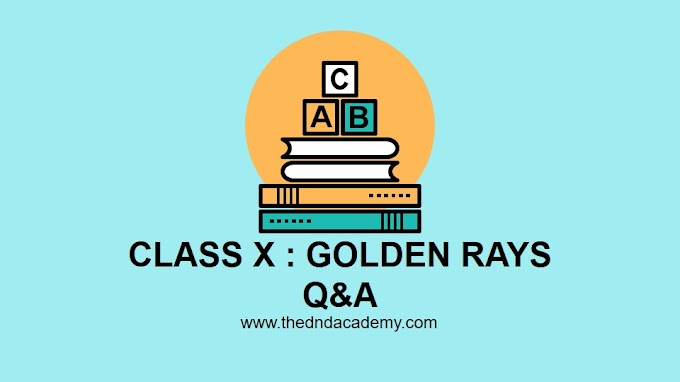आर्थिक अवधारणाएं एवं नियोजन
राष्ट्रीय आय - एक वित्त वर्ष में देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय.का योग राष्ट्रीय आय
कहलाती है।
वित्त वर्ष - भारत में वित्त वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
उत्पादन - उपयोगिता का सृजन तथा मूल्य वृद्धि का सृजन ही
उत्पादन होता है।
Note - राष्ट्रीय आय एक अर्थव्यवस्था की आर्थिक निष्पादकता का मौद्रिक माप है।
राष्ट्रीय आय की गणना एक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नांकित दृष्टि से
महत्त्वपूर्ण होती है –
(अ) राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की आर्थिक स्थिति तथा आर्थिक प्रगति का ज्ञान
होता है।
(आ) राष्ट्रीय आय के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना
कर सकते हैं।
(इ) इससे अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान एवं उनके सापेक्षिक
महत्त्व की जानकारी मिलती है।
(ई) राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर अर्थव्यवस्था के लिए भावी नीतियों का
निर्माण किया जा सकता है।
घरेलू साधन आय – देश की घरेलू सीमाओं के
अन्दर उत्पन्न होने वाली साधन आय घरेलू साधन आय कहलाती है।
राष्ट्रीय आय की अवधारणाए- सकल घरेलू
उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आदि।
सकल घरेलू उत्पाद – एक वित्त वर्ष
के दौरान देश के घरेलू सीमाओं में उत्पादित समस्त अन्तिम वस्तुओं और सेवाओं के
मौद्रिक मूल्यों का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है।
प्रति व्यक्ति आय – प्रति व्यक्ति
आय ज्ञात करने के लिए देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की जनसंख्या से विभाजित किया
जाता है –
प्रति व्यक्ति आय = राष्ट्रीय आय / जनसंख्या
भारत में राष्ट्रीय आय की गणना-
· भारत में राष्ट्रीय आय की प्रथम गणना श्री दादा भाई नौरोजी
द्वारा 1868 ई. में की गयी थी।
· भारत सरकार द्वारा श्री पी0 सी0 महालनोबिस की अध्यक्षता में
अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया।
· राष्ट्रीय आय समिति द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य
केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (Central Statistical
Organisation-CSO)
को सौंप दिया गया, जो वर्ष 1955 से प्रतिवर्ष CSO भारत में
राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कर रहा है।
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र
अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्र
प्राथमिक क्षेत्र – इस क्षेत्र में
उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें
प्राकृतिक संसाधनों को प्रत्यक्ष रूप से उपयोग में लेकर उत्पादन किया जाता हैं। जैसे-कृषि,
डेयरी, खनन इत्यादि।
· प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता
है।
द्वितीयक क्षेत्र – इस क्षेत्र में
उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है, जिनमें उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली
द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी
कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर सूत
कातना और कपड़ा बुनना, गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार
करना, मिट्टी से ईंटें बनाना इत्यादि।
·
यह क्षेत्र
क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए
इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है।
तृतीयक क्षेत्र – इस क्षेत्र में
उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में
सहयोग करती हैं। ये स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन
प्रक्रिया में सहयोग करती हैं। परिवहन, भण्डारण, संचार, बैंक
सेवाएं और व्यापार तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं।
· ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए
तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है।
अर्थव्यवस्था क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन –
(i) विकास की प्रारम्भिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही सबसे महत्त्वपूर्ण
क्षेत्र रहा है। धीरे-धीरे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और यह क्षेत्र समृद्ध
होता गया व पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा।
(ii) विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका
प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत से लोग कारखानों में काम करने लगे। कुल
उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्त्वपूर्ण हो गया।
(iii) कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्त्व बढ़ गया। अधिकांश
श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में नियोजित हैं।
उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्त्व –
पिछले वर्षों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई
है परन्तु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। भारत में तृतीयक
क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र
का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 85 प्रतिशत से अधिक है। ये क्षेत्र लगभग आधे लोगों
को रोजगार प्रदान करते हैं।
आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास
आर्थिक वृद्धि - समय के साथ-साथ राष्ट्रीय
आय तथा प्रति व्यक्ति आय में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि के रूप में
परिभाषित किया जाता है।
आर्थिक विकास - आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ
लोगों के जीवन की गुणवत्ता के अन्य आयामों में सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को
आर्थिक विकास कहा जाता है।
Note –
·
राष्ट्रों के
बीच तुलना करने के लिये कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। कुल आय की तुलना करने से
हमें यह ज्ञात नहीं होता है कि औसत व्यक्ति क्या कमा रहा है, इसीलिए
राष्ट्रीय आय की तुलना में औसत या प्रति व्यक्ति आय को अधिक महत्त्व प्रदान किया
जाता है।
किसी भी राष्ट्र के विकास के स्तर तथा कल्याण के मापक के रूप में आर्थिक विकास
को आर्थिक वृद्धि की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। इसका कारण निम्न अंतर आधार
पर स्पष्ट किया जा सकता है –
आर्थिक वृद्धि
|
आर्थिक विकास
|
आर्थिक वृद्धि के गुणात्मक आयाम नहीं होते हैं।
|
आर्थिक विकास की प्रक्रिया के गुणात्मक आयाम भी होते हैं।
|
यह मूल्यविहीन अवधारणा है।
|
आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है।
|
आर्थिक वृद्धि में सामाजिक, राजनैतिक, संस्थागत
इत्यादि स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों पर कोई विचार नहीं किया जाता हैं।
|
आर्थिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक एवं
राजनैतिक कल्याण को सुनिश्चित करती है।
|
सतत विकास या धारणीय विकास या पोषणीय विकास – प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाये रखते हुऐ जो आर्थिक विकास किया जाता
है वह सतत विकास कहलाता है।
समावेशी विकास - समावेशी विकास यह सुनिश्चित
करता है कि विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुँचने चाहिये।
·
यह एक व्यापक
अवधारणा है जो आय की समानता के साथ-साथ अवसर की समानता तथा जीवन के सभी आयामों में
समान मानवीय अधिकारों का समर्थन करती है।
मानव विकास -
मानव विकास की अवधारणा 1990 ई. में मानव विकास सूचकांक की रचना के साथ प्रारम्भ हुई।
महबूब उल हक के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तीन व्यापक
आयामों यथा ज्ञान, स्वास्थ्य (जीवन–प्रत्याशा) तथा जीवन-स्तर (प्रति व्यक्ति
आय) को शामिल करते हुऐ मानव विकास के स्तर को मापने के लिए एक सूचकांक तैयार किया
गया। यह राष्ट्रों के कल्याण और विकास के स्तर को मापने तथा विभिन्न राष्ट्रों के
बीच तुलना करने हेतु एक प्रभावी सूचकांक है।
PART-1